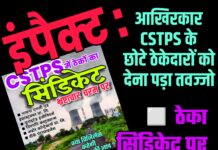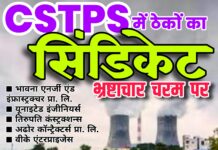संपादकीय
आज भारत में नागरिकता का सवाल सिर्फ कागज़ी नहीं रह गया है, यह अब अस्तित्व और सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है। असम से शुरू हुआ एनआरसी का जिन्न, अब गुरुग्राम, दिल्ली, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है। डर का यह माहौल बताता है कि हम एक खतरनाक दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां नागरिकों को उनके नाम, भाषा, धर्म और पहनावे के आधार पर “देशी या विदेशी” घोषित किया जा रहा है।
26 जुलाई को दिल्ली में जारी हुई 182 पन्नों की रिपोर्ट “Unmaking Citizens” बताती है कि किस तरह भारत की न्यायिक प्रणाली में नागरिकता के नाम पर एक अनदेखा, अनियमित और असंवेदनशील तंत्र काम कर रहा है। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के 1500 से अधिक फैसलों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। दस्तावेजों में मामूली त्रुटियों पर नागरिकता छीन लेना, चेहरे, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण निर्णय, बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया के लोगों को विदेशी ठहरा देना।
गुरुग्राम के सेक्टर 49 में बंगाली बस्ती में रह रहे लोग, जो 2020 से किराए पर रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब कुछ है। आज अचानक डरे हुए हैं, गांव की ओर लौट रहे हैं। उन पर बांग्लादेशी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है।
पुलिस पूछताछ कर रही है, गाड़ियों में उठा ले जा रही है, और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो भी बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के।
एक बच्चे का सवाल कि मेरी पढ़ाई, डिग्री और मेहनत का क्या होगा अगर हमें कल कुछ हो गया?, इस देश की सबसे बड़ी अदालतों, प्रशासन और पूरे समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। क्या आज नागरिक समाज इतना निर्जीव हो गया है कि जब बंगाली भाषा बोलने वाला कोई मजदूर डरा हुआ है, तो हम अपने एसी कमरों में चैन से रह सकते हैं?
भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक देश है। लेकिन आज मुसलमान होना, बांग्ला बोलना, गरीब होना, शक की बुनियाद बन गए हैं। जिन लोगों ने दशकों से गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों को बनाने में अपना खून-पसीना बहाया, आज वही लोग बिना किसी ठोस आधार के विदेशी घोषित किए जा रहे हैं।
क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांगे, तो आप क्या दिखाएंगे? क्या आपका आधार कार्ड काफ़ी होगा?, वोटर आईडी?, जन्म प्रमाण पत्र?, सुप्रीम कोर्ट के जज सुधांशु धुलिया तक कह चुके हैं कि वो खुद इस तरह के दस्तावेज देने में अक्षम होंगे। अगर सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठा व्यक्ति यह कह रहा है, तो एक आम मज़दूर कैसे साबित करेगा कि वह भारतीय है? नागरिकता का मुद्दा कोई छोटा मसला नहीं है। यह भारत के लोकतंत्र की नींव, समानता, न्याय और गरिमा पर सीधा हमला है। अगर आज यह राजनीति एक वर्ग पर प्रयोग हो रहा है, तो कल यह आप पर भी लागू हो सकता है।
किसी की भाषा, धर्म या नाम देखकर उसके भारतीय होने पर शक करना, देशभक्ति नहीं, घोर देशविरोध है। देशप्रेम यह है कि हर नागरिक अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, बंगाली हो या पंजाबी अपने देश में सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके।
हमें तय करना है कि हम अंधराष्ट्रवाद” की अफीम में डूबते रहेंगे या फिर “संवैधानिक नागरिकता” की मशाल जलाकर इस अंधकार को काटेंगे।
भारत की नागरिकता का सवाल अब केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि यह आम लोगों की अस्मिता, गरिमा और जीवन के अस्तित्व से जुड़ गया है। दस्तावेज़ों की गहराई में गुम होते चेहरों की कहानी, अब चिंता का विषय नहीं, बल्कि चेतावनी है कि कल यह संकट आपके दरवाज़े पर भी दस्तक दे सकता है।
जब बात नागरिकता की होती है तो उंगलियां सबसे पहले गरीब मुसलमानों की ओर उठती हैं। जिनकी चमचमाती जीवनशैली है, बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, उन पर किसी को शक नहीं होता। यह चयनात्मक भय और पूर्वाग्रह हमें एक खतरनाक सामाजिक दरार की ओर ले जा रहा है। असम में अब तक 165,992 लोगों को विदेशी घोषित किया गया। हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रक्रिया में खो दिया, लेकिन अंततः वे भारतीय साबित हुए। रहीम अली और हजारा खातून जैसे लोगों ने अपनी नागरिकता साबित करने में दशकों लगा दिए, सिर्फ दस्तावेज़ों की मामूली गलतियों के कारण उन्हें विदेशी ठहराया गया।
फॉरेनर ट्रिब्यूनल के हजारों फैसलों में कोई तारतम्यता नहीं है। एक ही प्रकार के दस्तावेज़ एक मामले में मान्य हैं और दूसरे में अमान्य। ट्रिब्यूनल के पास कोई स्थायी प्रक्रिया संहिता नहीं है। इसके अधिकांश सदस्य कार्यपालिका के आदेश से नियुक्त होते हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है।
महाराष्ट्र में चार मुसलमानों को बांग्लादेशी समझकर सीमा पार धकेल दिया गया, जबकि वे भारतीय नागरिक थे। बाद में दस्तावेज़ों के आधार पर उन्हें वापिस लाना पड़ा। उफा अली जैसे बुजुर्गों को नो-मैनस लैंड में घुटनों तक पानी में 12 घंटे खड़े रहना पड़ा, यह किसी लोकतांत्रिक देश की पहचान नहीं हो सकती। महिलाओं के पास अक्सर दस्तावेज़ नहीं होते या शादी के बाद नाम व पता बदलने से साक्ष्य की कड़ी टूट जाती है। उन्हें पंचायत या गांव के मुखिया के प्रमाण पर भरोसा करना पड़ता है, जिसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल बार-बार खारिज करता है।
आज भले ही यह संकट सीमित लगे, पर कल यह आपके विरोध या आलोचना के आधार पर भी आपके दरवाज़े आ सकता है। अगर सिस्टम को आप दूसरों के लिए मनमाना बनने देते हैं, तो कल वह आपके लिए भी मनमानी करेगा। भारत के करोड़ों नागरिकों की पहचान कागज़ के टुकड़ों में नहीं, उनके जीवन, व्यवहार और समाज में हिस्सेदारी से तय होनी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र का मूल्य न्यायप्रियता और मानवीयता से तय होता है, न कि उसके नागरिकों से बार-बार उनकी वफादारी साबित करने की मांग करके। हमें यह तय करना होगा कि हम सरकार का डर फैलाकर नागरिकता तय करना चाहते हैं, या संविधान का भरोसा देकर इसे संरक्षित करना चाहते हैं।
भारत में नागरिकता से जुड़े सवालों को सुलझाने के लिए जो कानूनी ढांचा अपनाया गया है, उसकी जड़ें आज़ादी से पहले के ब्रिटिश काल में मौजूद हैं। 1946 का फॉरेनर्स एक्ट आज भी उस सोच का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सरकार को पूर्ण अधिकार मिलते हैं, लेकिन नागरिक को मूलभूत कानूनी सुरक्षा नहीं। इस कानून की उत्पत्ति 1939 के फॉरेनर्स ऑर्डिनेंस और फिर 1940 और 1946 के फॉरेनर्स एक्ट से हुई थी। यह कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को, जिसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाए, बिना मुकदमे, बिना प्रक्रिया के हिरासत में ले सकती है, उसे देश से निकाल सकती है।
फॉरेनर्स एक्ट में विदेशी शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कौन विदेशी है और कौन भारतीय, इसका निर्धारण किस प्रक्रिया से होगा, यह एक्ट में स्पष्ट नहीं है। नतीजा यह कि निर्णय लेने वाली प्रशासनिक इकाई के पास अत्यधिक अधिकार, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का गठन कानून के तहत नहीं, बल्कि सरकारी प्रशासनिक आदेश से हुआ है। इसमें कार्यरत सदस्य जज की भूमिका में तो होते हैं, लेकिन उन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं। उनकी नियुक्ति, सेवा विस्तार और बर्खास्तगी सब कुछ राजनीतिक दखल से प्रभावित होती है।
गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा गठित चयन समिति सिर्फ 100 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर सदस्य चुनती है। ट्रिब्यूनल के सदस्यों को न तो पर्याप्त अनुभव की शर्तों में पाबंद किया गया है और न ही नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी है। 2021 में देखा गया कि पुलिस और गृह विभाग ने ट्रिब्यूनल सदस्यों की समीक्षा की, न कि न्यायपालिका ने। कई सदस्य इसलिए हटाए गए क्योंकि उन्होंने कम लोगों को विदेशी घोषित किया, जबकि जिन्होंने अधिक लोगों को विदेशी बताया, उन्हें सेवा विस्तार मिला। 221 सदस्यों को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था, जिन्हें बाद में एनआरसी का हवाला देकर हटा दिया गया। बिना वैधानिक आधार के। गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन बर्खास्तियों को चुनौती दी गई है, लेकिन अभी तक कोई पारदर्शी ढांचा नहीं बन पाया।
हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसलों की समीक्षा का दायरा सीमित कर दिया है, जिससे सिविल कोर्ट तक की भूमिका खत्म हो गई। हजारों फैसलों की समीक्षा में रिपोर्ट ने पाया कि अदालतें भी ट्रिब्यूनल की गलतियों का बचाव करती हैं, सुधार नहीं। जब लोगों के पास रोजगार नहीं, महंगाई से हाल बेहाल है, तब ऐसे कानूनों के जरिए लोगों के भीतर डर फैलाना, संदेह पैदा करना सत्ता का मनोवैज्ञानिक हथियार बन गया है। आज सवाल सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हर उस व्यक्ति पर उठने वाला है जो अपने दस्तावेज नहीं जुटा पाया। यह संकट सिर्फ सीमावर्ती राज्य असम का नहीं, कल आपके घर, मोहल्ले तक भी पहुंच सकता है।
क्या हर भारतीय अपने पूर्वजों के दस्तावेज प्रस्तुत कर पाएगा? क्या एक आम नागरिक यह चाहेगा कि सरकारी व्यवस्था इतनी मनमानी और अपारदर्शी हो जाए कि उसके भविष्य का फैसला कुछ महीनों के अनुबंध पर काम कर रहे अधिकारियों के हाथ में हो? यह बहस केवल बांग्ला भाषी मुसलमानों या घुसपैठियों की नहीं है। यह सवाल पूरे लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का है। जिस दिन यह मनमानी व्यवस्था बहुसंख्यक समाज तक पहुंचेगी, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी।
अब समय है चेतने का, नागरिकता की राजनीति के नाम पर खड़ी इस मनमानी प्रणाली के खिलाफ सवाल उठाने का।